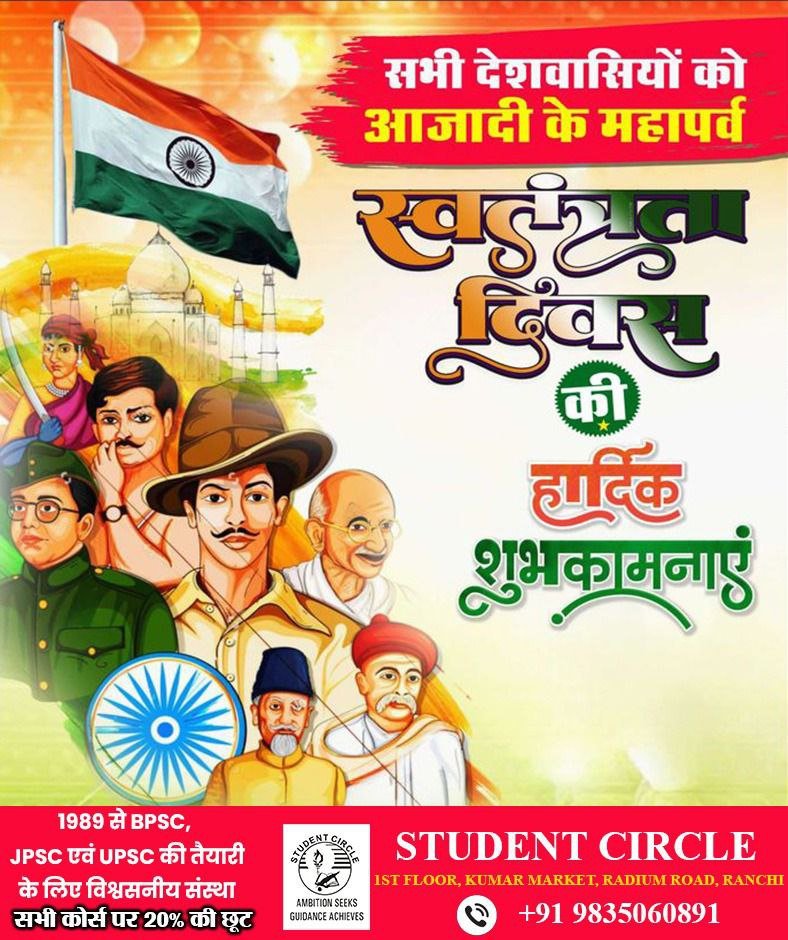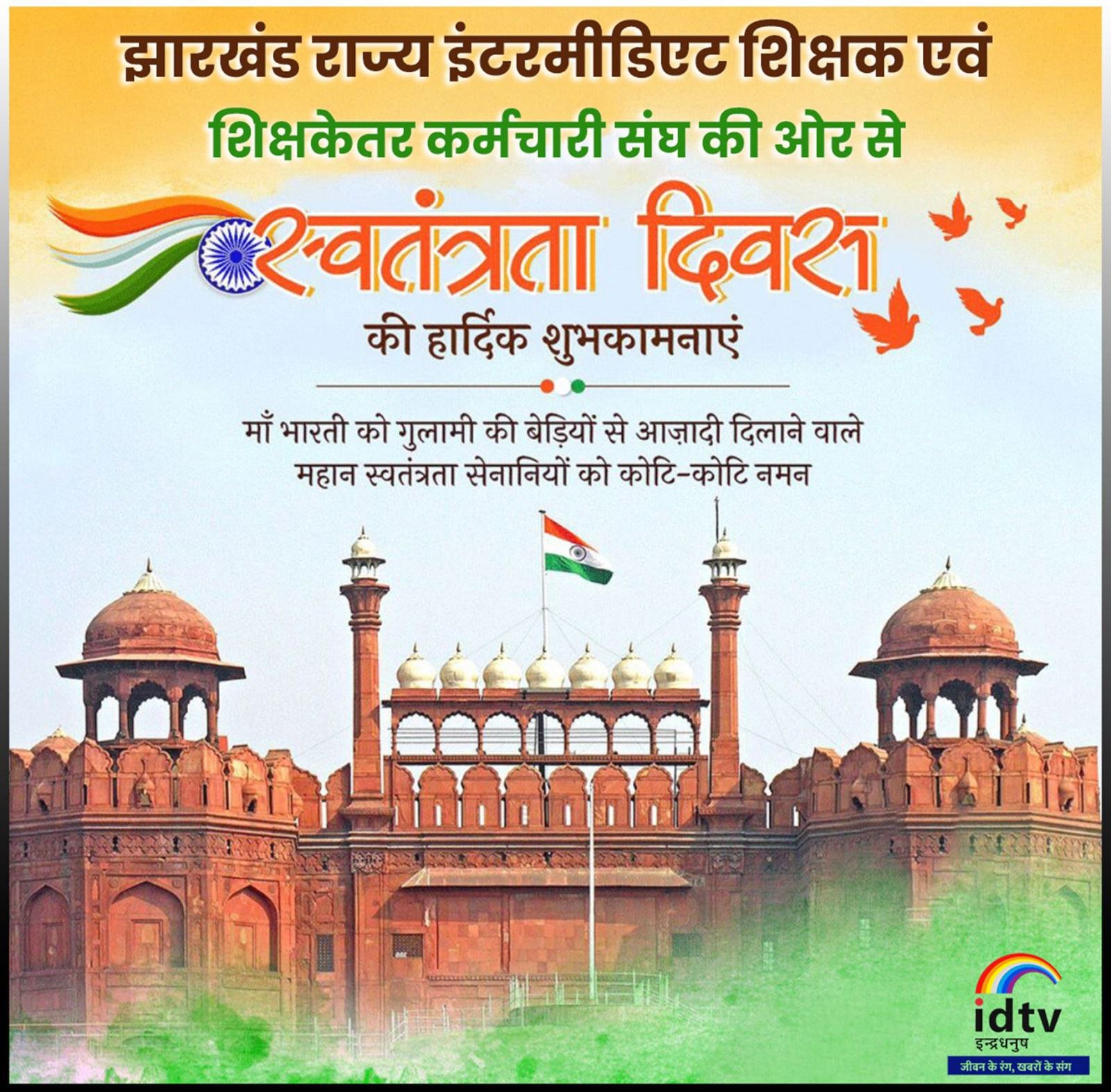रांची। पेसा कानून, यानी पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996, भारत सरकार का एक कानून है। यह कानून, अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को स्वशासन दिलाने के लिए बनाया गया था।
इस कानून के तहत, ग्राम सभाओं को ज़मीन, संसाधन, और स्थानीय विकास से जुड़े फ़ैसले लेने का अधिकार दिया गया है। पेसा कानून, भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के प्रावधानों से प्रेरित है। यह कानून, पांचवीं अनुसूची राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों में लागू किया गया था।
पेसा कानून के मुख्य उद्देश्य:
- आदिवासी आबादी को स्वशासन देना
- ग्राम शासन स्थापित करना
- आदिवासी परंपराओं और रीति-रिवाजों का संरक्षण करना
- आदिवासियों की ज़रूरतों के मुताबिक पंचायतों को मज़बूत बनाना
- आदिवासी समुदायों को अपने इलाकों में प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन और इस्तेमाल करने का अधिकार देना
- ग्राम सभाओं की सक्रिय भागीदारी से आदिवासी आबादी को शोषण से बचाना
हाईकोर्ट ने झारखंड लागू करने का दिया है निर्देशः
झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में पेसा कानून लागू करने का निर्देश दे रखा है। कोर्ट ने पंचायती राज अधिनियम और सरकार द्वारा प्रस्तावित पेसा रूल की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद ये आदेश जारी किया है।
संसद ने 1996 में पेसा एक्ट को पारित किया और राष्ट्रपति की अनुमति के बाद यह कानून बना, लेकिन झारखंड में आज तक यह कानून लागू नहीं हो पाया है। हालांकि राज्य की मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने एक बार लोगों को आश्वस्त किया है कि राज्य में यह कानून जल्द लागू होगा।
क्या है पेसा एक्ट 1996?
5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में पेसा एक्ट लागू करने की व्यवस्था है। वर्तमान में देश के कुल 10 राज्य 5वीं अनुसूची में आते हैं, जिनके नाम हैं -आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना।
इस अनुसूची में उन्हीं राज्यों को शामिल किया जाता है, जहां जनजातियों की आबादी अधिक है। पेसा एक्ट 1996 लागू होने के बाद झारखंड और ओडिशा को छोड़कर अन्य राज्यों ने इसे लागू कर दिया है।
पेसा अधिनियम, 1996 का उद्देश्य अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाना है। इस एक्ट के जरिए जनजातीय समुदाय को अपने स्थानीय स्वशासन से जोड़कर रखने और उसे सशक्त बनाने का प्रयास किया गया है।
पेसा एक्ट को संसद ने 1996 में पारित किया था और राष्ट्रपति ने इस एक्ट को अपनी मंजूरी 24 दिसंबर 1996 को देकर इसे कानून का रूप दिया था। इस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार पंचायतों से संबंधित प्रावधानों को 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में संशोधित रूप में लागू करना है।
पेसा एक्ट का उद्देश्यः
पेसा एक्ट 1996 उन राज्यों के लिए बनाया गया है जहां आदिवासी आबादी अधिक है और यह क्षेत्र आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने और इलाके के समुचित विकास के लिए पेसा एक्ट बनाया गया है।
पेसा एक्ट के जरिए इन इलाकों में प्रशासन की विशेष प्रणाली विकसित करने की कोशिश की गई है, ताकि क्षेत्र का समुचित विकास हो सके। इसकी आवश्यकता इसलिए महसूस की गई क्योंकि इन राज्यों में जो प्रशासनिक मशीनरी काम कर रही है, उनका विस्तार इन क्षेत्रों तक नहीं हो पाता है। इस कानून का उद्देश्य पंचायतों के संवैधानिक प्रावधानों और आदिवासियों के विशेष पारंपरिक अधिकारों के बीच सामंजस्य करनाय़
पेसा एक्ट के उद्देश्य इस प्रकार हैं-
- पंचायतों से संबंधित भारतीय संविधान के भाग IX के प्रावधानों को कुछ संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों तक ले जाना
- आदिवासी आबादी को स्वशासन प्रदान करना
- ग्राम शासन स्थापित करना और ग्रामसभा को शक्तिशाली बनाना-आदिवासियों के पारंपरिक प्रथाओं के अनुसार प्रशासनिक ढांचा विकसित करना
- आदिवासियों की परंपराओं और रीति-रिवाजों का संरक्षण
- आदिवासियों की आवश्यकताओं के अनुसार पंचायतों को शक्तिशाली बनाना
- प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण पेसा अधिनियम आदिवासी समुदायों को उनके क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों, जैसे भूमि, जल और जंगलों के प्रबंधन और उपयोग पर नियंत्रण प्रदान करता है।
पेसा एक्ट, 1996 में क्या हैं प्रावधानः
पेसा एक्ट 1996 में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता अवनीश रंजन मिश्रा बताते हैं कि पेसा एक्ट लागू होने से अनुसूचित क्षेत्रों के लोगों को काफी लाभ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।
जो ग्राम प्रधान होगा उसमें तमाम शक्तियां निहित होंगी यानी उसे प्रशासनिक कार्यों से संबंधित तमाम अधिकार प्राप्त होंगे. यानी एक पंक्ति में कहें तो उसके पास उपायुक्त के बाद सबसे अधिक अधिकार होंगे।
ग्राम सभा काफी मजबूत होगी, इस ग्राम सभा में गांव के हर वो व्यक्ति शामिल होंगे जिनके नाम मतदाता सूची में शामिल होंगे। ग्राम सभाएं अपने लोगों के पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार काम करेगी और इलाके में प्रशासनिक कार्य संपन्न होंगे।
ग्राम सभाएं क्या-क्या कर पाएंगीः
- ग्राम सभाएं सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाओं को मंजूरी देंगी।
- प्रत्येक पंचायत को योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए निधियों के उपयोग का प्रमाण पत्र ग्राम सभा से प्राप्त करना होगा।
- विकास परियोजनाओं के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण करने से पहले ग्राम सभा या पंचायतों से परामर्श किया जाएगा।
- पेसा-एक्ट और पंचायती राज अधिनियम में विवाद क्या?
पंचायती राज अधिनियम और सरकार द्वारा प्रस्तावित पेसा रूल की वैधता को चुनौती देने वालों में वाल्टर कंडुलना और रॉबर्ट मिंज शामिल हैं। रॉबर्ट मिंज ने इस केस में कोर्ट में पक्ष भी रखा है, इन्होंने कहा कि वे पंचायती राज अधिनियम का पूरी तरह विरोध करते हैं, क्योंकि यह अधिनियम 5वीं अनुसूची में शामिल राज्यों में लागू नहीं किया जा सकता है।
पेसा एक्ट पास होने के बाद पांचवीं अनुसूची के राज्यों ने नियमावली बनाकर इसे लागू कर दिया, लेकिन झारखंड में पेसा एक्ट को लागू करने के लिए नियमावली बनाने की बजाय नया कानून पंचायती राज अधिनियम लागू कर दिया गया।
पेसा एक्ट झारखंड के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके जरिए ही यहां की प्राचीन स्वशासन व्यवस्था को सुरक्षित किया जा सकता है। इस एक्ट के जरिए ही यहां के रीति-रिवाज भी सुरक्षित रहेंगे।
आदिवासियों की प्राचीन व्यवस्था में त्रिस्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था है, जिसे पंचायती राज अधिनियम में दरकिनार किया गया है। रॉबर्ट मिंज ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों का प्रधान राज्यपाल होता है, लेकिन राज्यपाल ने पेसा एक्ट को लागू करने की दिशा में कोई ठोस कार्य नहीं किया, इसलिए अगले कुछ समय में हम उनके खिलाफ पीआईएल दाखिल करेंगे।
अनुसूचित क्षेत्रों के लिए है अलग कानून व्यवस्था : वाल्टर कंडुलना
वाल्टर कंडुलना का कहना है कि पंचायती राज अधिनियम हमारी प्राचीन शासन व्यवस्था के खिलाफ है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। जब देश में अनुसूचित क्षेत्रों के लिए अलग से कानून बनाए गए हैं, तो झारखंड को उससे अलग क्यों रखा जाए।
हमारी लड़ाई इसी को लेकर है, लेकिन अब तक पेसा कानून देश में लागू नहीं हो पाया है। हमने एक नियमावली भी प्रस्तावित की है, जिसके जरिए संवैधानिक तरीके से पेसा कानून झारखंड में लागू किया जा सकता है।
अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज अधिनियम लागू करना असंवैधानिक नहीं : विभाग
पंचायती राज विभाग झारखंड का मानना है कि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज अधिनियम लागू करना कहीं से भी असंवैधानिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों में यह बात साबित भी हो चुकी है। 2010 में सुप्रीम के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस केजी बालकृष्णन और पी सदाशिवम ने अपने फैसले में पंचायती राज अधिनियम की धारा 21 (बी), 40 (बी) और 55 (बी) को संवैधानिक बताया था।
निशा उरांव कहती हैं कि यह संभव नहीं है कि किसी अधिनियम का कोई सेक्शन संवैधानिक हो और वह कानून असंवैधानिक। झारखंड में जो भी पेसा रूल बना है वह पेसा एक्ट, 1996 के तहत ही बना है, इसमें अलग से कोई व्यवस्था नहीं की गई है।
अगर किसी को कोई आपत्ति है तो उन्हें अपनी आपत्ति लिखित रूप में दर्ज करानी चाहिए, हम उसे कानून मंत्रालय के पास भेजेंगे।
पेसा रूल और पंचायती राज अधिनियम में घालमेल का हो रहा विरोध : ग्लैडसन डुंगडुंग
सामाजिक कार्यकर्ता ग्लैडसन डुंगडुंग का कहना है कि पेसा रूल को लेकर विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि पंचायती राज अधिनियम और इसमें घालमेल कर दिया गया है। पेसा एक्ट के कुछ प्रावधान तो पेसा रूल में शामिल किए गए हैं, लेकिन सभी प्रावधान इसमें नहीं लिए गए हैं।
1996 में जब पेसा एक्ट पास किया गया, उस वक्त राज्य सरकारों को यह कहा गया था कि वे एक साल के अंदर अपनी–अपनी नियमावली बना लें, उस वक्त बिहार राज्य था और पेसा रूल नहीं बना। जब झारखंड अलग राज्य बना तो 2001 में पंचायती राज अधिनियम पूरे राज्य में लागू कर दिया, जबकि अनुसूचित क्षेत्रों में पेसा एक्ट लागू करना चाहिए था।
पंचायती राज अधिनियम में पेसा एक्ट के कुछ प्रावधान शामिल करके घालमेल कर दिया गया है, इसलिए विरोध हो रहा है। पेसा एक्ट पूरे झारखंड में लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन अनुसूचित क्षेत्रों में इसे लागू किया जाना चाहिए।
क्या है पंचायती राज अधिनियम 2001
पंचायती राज अधिनियम 2001 के तहत राज्य में पंचायत चुनाव की शुरुआत हुई। अनुसूचित क्षेत्रों और गैर अनुसूचित क्षेत्रों में अलग-अलग कानून की व्यवस्था की गई है और उनमें अलग-अलग तरीके से पंचायती राज चलाने की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज अधिनियम 2001 का उद्देश्य स्थानीय स्वशासन को बढ़ाना है।
इसे भी पढ़ें
पेसा कानून को झारखंड में जल्द लागू कराएं सीएम हेमंत : राज्यपाल