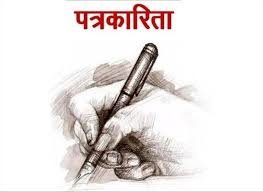हिन्दी पत्रकारिता की वर्तमान स्थिति
हिन्दी पत्रकारिता की वर्तमान स्थिति संभावनाओं और चुनौतियों की दहलीज पर खड़े युवा की तरह है।
आज जहां हिन्दी पत्रकारिता बदलाव के तमाम अवसरों का लाभ उठा रही है और सोशल मीडिया पर मजबूती से कदम रख रही है।
वहीं, पत्रकारिता के धुरंधर अब यू-ट्यूब चैनलों पर नजर आ रहे हैं। चाहे वो दीपक शर्मा हो या पुण्य प्रसून वाजपेयी या फिर रवीश कुमार या अजीत अंजुम।
सभी मुख्यधारा की पत्रकारिता से यू-ट्यूब चैनल की ओर टर्न कर गए हैं। प्रिंट पत्रकारिता की बात करें तो अखबार जो कभी भाषा सीखने और सिखाने का जरिया थे साख और विश्वसनीयता के संकट से गुजर रहे हैं।
कहने को तो देश में हजारों की संख्या में अखबार निकलते हैं पर प्रिंट पत्रकारिता में चुनिंदा अखबार ही बड़ी संख्या में छपते और बिकते हैं।
सोशल मीडिया के दौर में यू-ट्यूब चैनलों की संख्या बढ़ रही है और दर्शक भी इन्हें पसंद कर रहे हैं।
मुख्य धारा के टीवी चैनल गोदी मीडिया कहे जाने लगे हैं और उनकी साख पर सवाल उठने लगे हैं।
यह कहना समीचीन होगा कि जैसे हर पेशे में गिरावट आयी है उसी तरह पत्रकारिता भी गिरावट का सामना कर रही है।
पर पत्रकारिता की वर्तमान स्थिति पर चर्चा से पहले पत्रकारिता की इतिहास यात्रा से रुबरु होना जरूरी है।
हिन्दी पत्रकारिता की कहानी
हिन्दी पत्रकारिता की कहानी भारतीय राष्ट्रीयता की कहानी है। हिन्दी पत्रकारिता के आदि उन्नायक जातीय चेतना, युगबोध और अपने महत् दायित्व के प्रति पूर्ण सचेत थे।
कदाचित् इसलिए विदेशी सरकार की दमन-नीति का उन्हें शिकार होना पड़ा था, उसके नृशंस व्यवहार की यातना झेलनी पड़ी थी।
उन्नीसवीं शताब्दी में हिन्दी गद्य-निर्माण की चेष्टा और हिन्दी-प्रचार आन्दोलन अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थितियों में भयंकर कठिनाइयों का सामना करते हुए भी कितना तेज और पुष्ट था इसका साक्ष्य ‘भारतमित्र’ (सन् 1878 ई, में) ‘सार सुधानिधि’ (सन् 1879 ई.) और ‘उचित वक्ता’ (सन् 1880 ई.) के जीर्ण पृष्ठों पर मुखर है।
भारत में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी भाषा का अखबार, उदंत मार्तंड (द राइजिंग सन), 30 मई 1826 को शुरू हुआ।
इस दिन को “हिंदी पत्रकारिता दिवस” के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसने हिंदी भाषा में पत्रकारिता की शुरुआत को चिह्नित किया था।
वर्तमान में हिन्दी पत्रकारिता ने अंग्रेजी पत्रकारिता के दबदबे को खत्म कर दिया है। पहले देश-विदेश में अंग्रेजी पत्रकारिता का दबदबा था लेकिन आज हिन्दी भाषा का झण्डा चहुंदिश लहरा रहा है। 30 मई को ‘हिन्दी पत्रकारिता दिवस’ के रूप में मनाया जाता है।
पत्रकारिता का जन्म
भारतवर्ष में आधुनिक ढंग की पत्रकारिता का जन्म अठारहवीं शताब्दी के चतुर्थ चरण में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में हुआ।
1780 ई. में प्रकाशित हिके (Hickey) का “कलकत्ता गज़ट” कदाचित् इस ओर पहला प्रयत्न था।
हिंदी के पहले पत्र उदंत मार्तण्ड (1826) के प्रकाशित होने तक इन नगरों की ऐंग्लोइंडियन अंग्रेजी पत्रकारिता काफी विकसित हो गई थी।
इन अंतिम वर्षों में फारसी भाषा में भी पत्रकारिता का जन्म हो चुका था। 18वीं शताब्दी के फारसी पत्र कदाचित् हस्तलिखित पत्र थे।
1801 में ‘हिंदुस्थान इंटेलिजेंस ओरिऐंटल ऐंथॉलॉजी’ नाम का जो संकलन प्रकाशित हुआ उसमें उत्तर भारत के कितने ही “अखबारों” के उद्धरण थे।
1810 में मौलवी इकराम अली ने कलकत्ता से लीथो पत्र “हिंदोस्तानी” प्रकाशित करना आरंभ किया।
1816 में गंगाकिशोर भट्टाचार्य ने “बंगाल गजट” का प्रवर्तन किया। यह पहला बंगला पत्र था। बाद में श्रीरामपुर के पादरियों ने प्रसिद्ध प्रचारपत्र “समाचार दर्पण” को (27 मई 1818) जन्म दिया।
इन प्रारंभिक पत्रों के बाद 1823 में हमें बँगला भाषा के ‘समाचारचंद्रिका’ और “संवाद कौमुदी”, फारसी उर्दू के “जामे जहाँनुमा” और “शमसुल अखबार” तथा गुजराती के “मुंबई समाचार” के दर्शन होते हैं।
यह स्पष्ट है कि हिंदी पत्रकारिता बहुत बाद की चीज नहीं है। दिल्ली का “उर्दू अखबार” (1833) और मराठी का “दिग्दर्शन” (1837) हिंदी के पहले पत्र “उदंत मार्तंड” (1826) के बाद ही आए।
“उदंत मार्तंड” के संपादक पंडित जुगलकिशोर थे। यह साप्ताहिक पत्र था। पत्र की भाषा पछांही हिंदी रहती थी, जिसे पत्र के संपादकों ने “मध्यदेशीय भाषा” कहा है।
प्रिंट मीडिया
आधुनिक काल में खासकर 90 के दशक में भारतीय भाषाओं के अखबारों, हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण आदि के नगरों-कस्बों से कई संस्करण निकलने शुरू हुए।
जहां पहले महानगरों से अखबार छपते थे, भूमंडलीकरण के बाद आयी नई तकनीक, बेहतर सड़क और यातायात के संसाधनों की सुलभता की वजह से छोटे शहरों, कस्बों से भी नगर संस्करण का छपना आसान हो गया।
साथ ही इन दशकों में ग्रामीण इलाकों, कस्बों में फैलते बाजार में नई वस्तुओं के लिए नये उपभोक्ताओं की तलाश भी शुरू हुई।
हिंदी के अखबार इन वस्तुओं के प्रचार-प्रसार का एक जरिया बन कर उभरा है। साथ ही साथ अखबारों के इन संस्करणों में स्थानीय खबरों को प्रमुखता से छापा जाता है।
इससे अखबारों के पाठकों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। मीडिया विशेषज्ञ सेवंती निनान ने इसे ‘हिंदी की सार्वजनिक दुनिया का पुनर्विष्कार’ कहा है।
वे लिखती हैं, “प्रिंट मीडिया ने स्थानीय घटनाओं के कवरेज द्वारा जिला स्तर पर हिंदी की मौजूद सार्वजनिक दुनिया का विस्तार किया है और साथ ही अखबारों के स्थानीय संस्करणों के द्वारा अनजाने में इसका पुनर्विष्कार किया है।
1990 में राष्ट्रीय पाठक सर्वेक्षण की रिपोर्ट बताती थी कि पांच अगुवा अखबारों में हिन्दी का केवल एक समाचार पत्र हुआ करता था।
पिछले (सर्वे) ने साबित कर दिया कि हम कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बार (2010) सबसे अधिक पढ़े जाने वाले पांच अखबारों में शुरू के चार हिंदी के हैं।
एक उत्साहजनक बात और भी है कि आईआरएस सर्वे में जिन 42 शहरों को सबसे तेजी से उभरता माना गया है, उनमें से ज्यादातर हिन्दी हृदय प्रदेश के हैं।
मतलब साफ है कि अगर पिछले तीन दशक में दक्षिण के राज्यों ने विकास की जबरदस्त पींगें बढ़ाईं तो आने वाले दशक हम हिन्दी वालों के हैं।
ऐसा नहीं है कि अखबार के अध्ययन के मामले में ही यह प्रदेश अगुवा साबित हो रहे हैं। आईटी इंडस्ट्री का एक आंकड़ा बताता है कि हिन्दी और भारतीय भाषाओं में नेट पर पढ़ने-लिखने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है।
मतलब साफ है। हिन्दी की आकांक्षाओं का यह विस्तार पत्रकारों की ओर भी देख रहा है। प्रगति की चेतना के साथ समाज की निचली कतार में बैठे लोग भी समाचार पत्रों की पंक्तियों में दिखने चाहिए।
पिछले आईएएस, आईआईटी और तमाम शिक्षा परिषदों के परिणामों ने साबित कर दिया है कि हिन्दी भाषियों में सबसे निचली सीढ़ियों पर बैठे लोग भी जबरदस्त उछाल के लिए तैयार हैं।
तकनीकी विकास को साथ-साथ जनसंचार माध्यमों यथा हिन्दी पत्रकारिता के रूख में तेजी से परिवर्तन देखने को मिला है।
तकनीकी के विस्तार से हिन्दी पत्रकारिता के विस्तार में मदद मिली है। हिन्दी समाचार चैनल, समाचार पत्रों के साथ-साथ हिन्दी में समाचार वेबसाइट के कारण हिन्दी पत्रकारिता का दायरा बढ़ा है।
हिन्दी पत्रकारिता को व्यवसायिक कलेवर में ढाला जा चुका है। वहीं तमाम समानान्तर माध्यम भी कार्य कर रहे है, जो व्यवसायिकता से अभी परे है।
यह समय के साथ लगातार विकसीत हो रहा है। तकनीकी के कारण सूचनाओं पर लगने वाली बंदिशे कम हुई है और लोगो तक अबाध सूचना का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इन सबके चलते हिन्दी पत्रकारिता ने नये दौर मे प्रवेश किया है।
21वीं शताब्दी सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। आधुनिक संचार तकनीकी का मूल आधार इन्टरनेट है।
कलमविहीन पत्रकारिता के इस युग में इन्टरनेट पत्रकारिता ने एक नए युग का सूत्रपात किया है।
वेब पत्रकारिता
वेब पत्रकारिता को हम इन्टरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता के नाम के जानते है।
यह कम्प्यूटर और इंटरनेट द्वारा संचालित एक ऐसी पत्रकारिता है, जिसकी पहुँच किसी एक पाठक, एक गांव, एक प्रखण्ड, एक प्रदेश, एक देश तक नहीं अपितु समूचे विश्व तक है।
प्रिंट मीडिया से यह रूप में भी भिन्न है इसके पाठकों की संख्या को परिसीमित नहीं किया जा सकता है।
इसकी उपलब्धता भी सर्वाधिक है। इसके लिए मात्र इन्टरनेट और कम्प्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल की जरूरत होती है।
इंटरनेट वेब मीडिया की सर्वव्यापकता को भी चरितार्थ करती है जिसमें खबरें दिन के चौबीसों घण्टे और हफ्ते के सातों दिन उपलब्ध रहती हैं वेब पत्रकारिता की सबसे बड़ी खासियत है उसका वेब यानी तरंगों पर आधारित होना।
इसमें उपलब्ध किसी दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पत्र-पत्रिका को सुरक्षित रखने के लिए किसी आलमीरा या लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं होती।
समाचार पत्रों और टेलीविजन की तुलना में इंटरनेट पत्रकारिता की उम्र बहुत कम है लेकिन उसका विस्तार बहुत तेजी से हुआ है।
उल्लेखनीय है कि भारत में इंटरनेट की सुविधा 1990 के मध्य में मिलने लगी। इस विधा में कुछ समय पहले तक अंग्रेजी का एकाधिकार था लेकिन विगत दशकों में हिन्दी ने भी अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज की है।
इंदौर से प्रकाशित समाचार पत्र ‘नई दुनिया’ ने हिन्दी का पहला वेब पोर्टल ‘वेब दुनिया’ के नाम से शुरू किया।
अब तो लगभग सभी समाचार पत्रों का इंटरनेट संस्करण उपलब्ध है। चेन्नई का ‘द हिन्दू’ पहला ऐसा भारतीय अखबार है जिसने अपना इंटरनेट संस्करण वर्ष 1995 ई. में शुरू किया।
इसके तीन साल के भीतर यानी वर्ष 1998 ई. तक लगभग 48 समाचार पत्र ऑन-लाइन हो चुके थे।
ये समाचार पत्र केवल अंग्रेजी में ही नहीं अपितु हिन्दी सहित अन्य भारतीय भाषाओं जैसे मलयालम, तमिल, मराठी, गुजराती आदि में थे।
आकाशवाणी ने 02 मई 1996 ‘ऑन-लाइन सूचना सेवा’ का अपना प्रायोगिक संस्करण इंटरनेट पर उतारा था।
एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2006 ई. के अन्त तक देश के लगभग सभी प्रतिष्ठित समाचार पत्रों एवं टेलीविजन चैनलों के पास अपना इंटरनेट संस्करण भी है जिसके माध्यम से वे पाठकों को ऑन-लाइन समाचार उपलब्ध करा रहे हैं।
संक्षेप में कहा जाए तो पत्रकारिता चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी राह बना रही है।
इसे भी पढ़ें