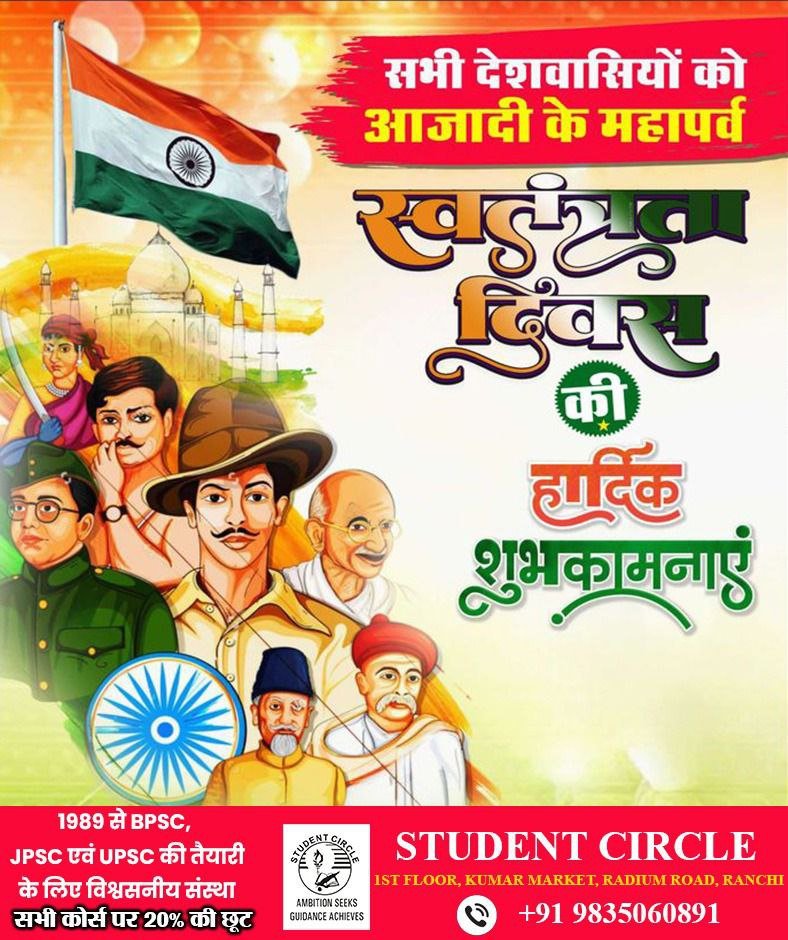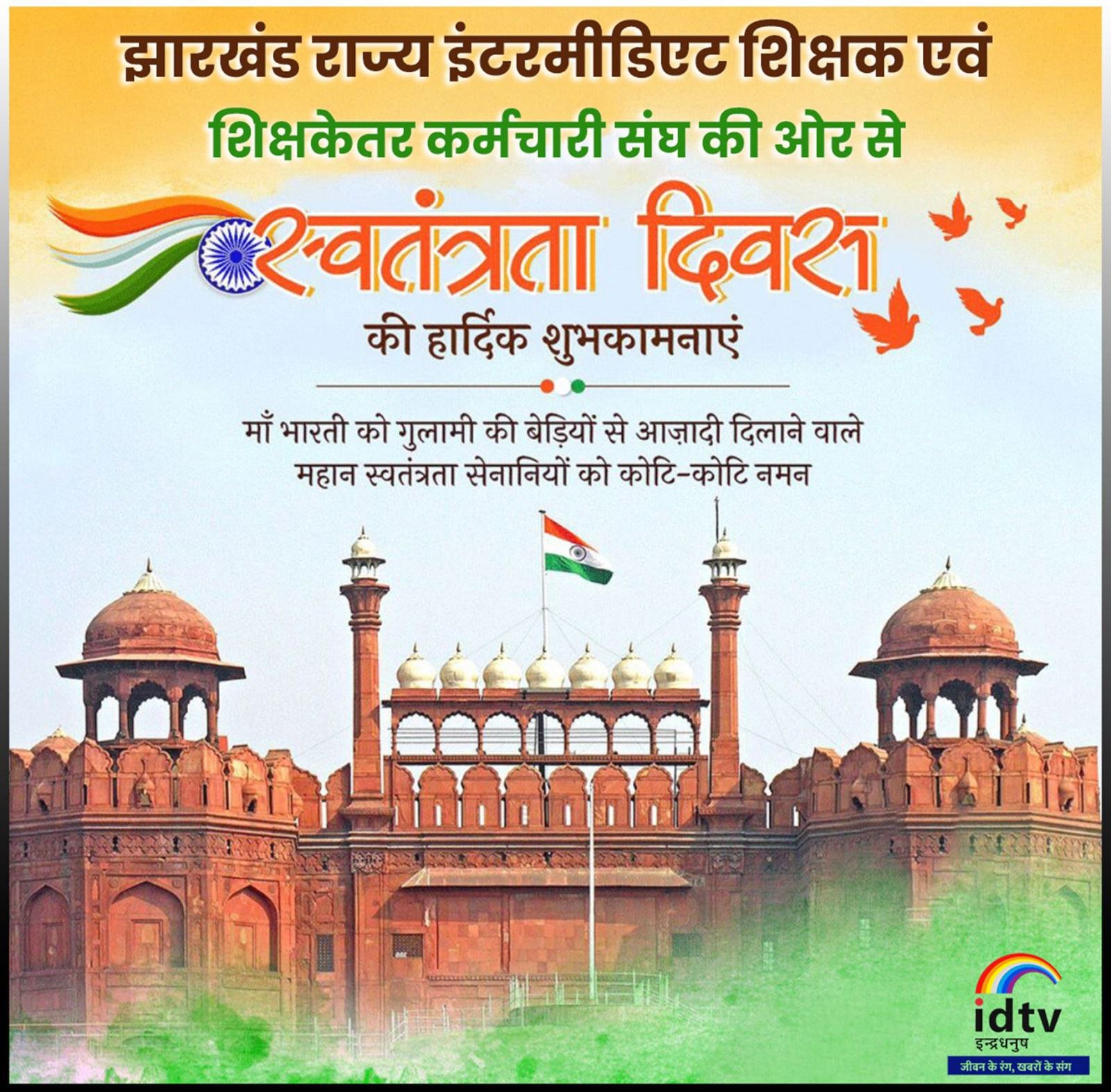गौतम बुद्ध [Gautam Buddha]
पूरी दुनिया को शांति, प्रेम, त्याग और सद्भावना का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा गौतम बुद्ध का जीवन प्रेरणादायक है।
राजा के बेटे होते हुए भी उन्होंने भिक्षु रूपी जीवन को चुना। उन्होंने तप से जो ज्ञान प्राप्त किया उसे शिक्षाओं के रूप में अपने शिष्यों को दिया। उनकी शिक्षाएं आज भी मानवता का पथ प्रदर्शन कर रही हैं।
गौतम बुद्ध
गौतम बुद्ध को भगवान बुद्ध और महात्मा बुद्ध आदि नामों से भी जाना जाता है। वे विश्व प्रसिद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं।
गौतम बुद्ध का जन्म 563 ई. पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था।
सिद्धार्थ ने गुरू विश्वामित्र के पास वेद और उपनिषद् तो पढ़े ही, राजकाज और युद्ध-विद्या की भी शिक्षा ली।
सिद्धार्थ के मन में बचपन से ही करुणा भरी थी। उनसे किसी भी प्राणी का दुख नहीं देखा जाता था। महात्मा बनने से पहले बुद्ध एक राजा थे।
वो बचपन से ही ऐसे प्रश्नों के उत्तर की तलाश में खोए रहते थे जिनका जवाब बड़े-बड़े संत और महात्माओं के पास भी नहीं था।
बुद्ध विवाह के बाद ही अपने परिवार को छोड़कर सत्य की तलाश में निकल पड़े थे और ज्ञान की प्रप्ति की। बुद्ध के उपदेश आज भी लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं।
ये हैं गौतम बुद्ध की शिक्षाएं
यदि आप वास्तव में ही अपने आप से प्रेम करते हैं,तो आप कभी भी दूसरों को दुःख नहीं पहुंचा सकते।
अपना रास्ता स्वयं बनाएं–हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इसलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता।
स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है,संतोष सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे बड़ा सम्बन्ध है।
अच्छी चीजों के बारे में सोचें– हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। इसलिए सकारात्मक बातें सोचें और खुश रहें।
आकाश में पूरब और पश्चिम का कोई भेद नहीं है,लोग अपने मन से भेदभाव को जन्म देते हैं और फिर विश्वास करते हैं कि यह सच है।
आपको क्रोधित होने के लिए दंड नहीं दिया जायेगा,बल्कि आपका क्रोध खुद आपको दंड देगा।
इंसान के अंदर ही शांति का वास होता है,उसे बाहर ना तलाशें।
एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रौशन किए जा सकते हैं,फिर भी उस दीपक की रौशनी कम नहीं होती। उसी तरह खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, कम नहीं होतीं।
क्रोधित रहना,जलते हुए कोयले को किसी दूसरे व्यक्ति पर फेंकने की इच्छा से पकड़े रहने के समान है, यह सबसे पहले आप को ही जलाता है।
दूसरों के सामने कुछ भी साबित करने से पहले यह जरूरी है कि हम खुद को साबित करें। हर इंसान की प्रतिस्पर्धा पहले खुद से होती है।
खुशी हमारे दिमाग में है- खुशी,पैसों से खरीदी गई चीजों में नहीं, बल्कि इस बात में है कि हम कैसा महसूस करते हैं। वास्तव में खुशी हमारे मस्तिष्क में है।
घृणा से घृणा कभी खत्म नहीं हो सकती। घृणा को केवल प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। यह शास्वत सत्य है।
जिस तरह एक मोमबत्ती बिना आग के खुद नहीं जल सकती,उसी तरह एक इंसान बिना अध्यात्म के जीवित नहीं रह सकता।
तीन चीजों को लम्बी अवधि तक छुपाया नहीं जा सकता,सूर्य, चन्द्रमा और सत्य।
भूतकाल में मत उलझो,भविष्य के सपनों में मत खो जाओ, वर्तमान पर ध्यान दो, यही खुश रहने का रास्ता है।
मैं कभी नहीं देखता की क्या किया जा चुका है;मैं हमेशा देखता हूँ कि क्या किया जाना बाकी है।
हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर है आप खुद को जीत लें।फिर वो जीत आपकी अपनी होगी, जिसे कोई आपसे नहीं छीन सकता।
हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है–हर अनुभव महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं।
हर इंसान को यह अधिकार है कि वह अपनी दुनिया की खोज स्वयं करे।
हर दिन की अहमियत समझें– इंसान हर दिन एक नया जन्म लेता है एक नए मकसद को पूरा करने के लिए है, इसलिए एक- एक दिन की अहमियत समझें।
बुद्ध दर्शन के सकारात्मक पहलू
बुद्ध के दर्शन का सबसे महत्त्वपूर्ण विचार ‘आत्म दीपो भवः’ अर्थात ‘अपने दीपक स्वयं बनो’।
इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य या नैतिक-अनैतिक प्रश्न का निर्णय स्वयं करना चाहिये।
यह विचार इसलिये महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह ज्ञान और नैतिकता के क्षेत्र में एक छोटे से बुद्धिजीवी वर्ग के एकाधिकार को चुनौती देकर हर व्यक्ति को उसमें प्रविष्ट होने का अवसर प्रदान करता है।
बुद्ध के दर्शन का दूसरा प्रमुख विचार ‘मध्यम मार्ग’ के नाम से जाना जाता है। सूक्ष्म दार्शनिक स्तर पर तो इसका अर्थ कुछ भिन्न है, किंतु लौकिकता के स्तर पर इसका अभिप्राय सिर्फ इतना है कि किसी भी प्रकार के अतिवादी व्यवहार से बचना चाहिये।
बुद्ध दर्शन का तीसरा प्रमुख विचार ‘संवेदनशीलता’ है। यहाँ संवेदनशीलता का अर्थ है दूसरों के दुखों को अनुभव करने की क्षमता।
वर्तमान में मनोविज्ञान जिसे समानुभूति (Empathy) कहता है, वह प्रायः वही है जिसे भारत में संवेदनशीलता कहा जाता रहा है।
बुद्ध दर्शन का चौथा प्रमुख विचार यह है कि वे परलोकवाद की बजाय इहलोकवाद पर अधिक बल देते हैं।
गौरतलब है कि बुद्ध के समय प्रचलित दर्शनों में चार्वाक के अलावा लगभग सभी दर्शन परलोक पर अधिक ध्यान दे रहे थे।
उनके विचारों का सार यह था कि इहलोक मिथ्या है और परलोक ही वास्तविक सत्य है। इससे निरर्थक कर्मकांडों तथा अनुष्ठानों को बढ़ावा मिलता था।
बुद्ध ने जानबूझकर अधिकांश पारलौकिक धारणाओं को खारिज किया।
बुद्ध दर्शन का पाँचवा प्रमुख विचार यह है कि वे व्यक्ति को अहंकार से मुक्त होने की सलाह देते हैं।
अहंकार का अर्थ है ‘मैं’ की भावना। यह ‘मैं’ ही अधिकांश झगड़ों की जड़ है। इसलिये व्यक्तित्व पर अहंकार करना एकदम निरर्थक है।
बुद्ध दर्शन का छठा प्रमुख विचार ह्रदय परिवर्तन के विश्वास से संबंधित है। बुद्ध को इस बात पर अत्यधिक विश्वास था कि हर व्यक्ति के भीतर अच्छा बनने की संभावनाएँ होती हैं, ज़रूरी यह है की उस पर विश्वास किया जाए और उसे समुचित परिस्थितियाँ प्रदान की जाएँ।
बुद्ध दर्शन के नकारात्मक पहलू
बुद्ध का सबसे कमज़ोर विचार उनका यह विश्वास है कि संपूर्ण जीवन दुखमय है। उन्होंने जो चार आर्य सत्य बताए हैं, उनमें से पहला ‘सर्वम दुखम’ है अर्थात सबकुछ दुखमय है।
इस बिंदु पर बुद्ध एकतरफा झुके हुए नज़र आते हैं जबकि जीवन को न तो सिर्फ दुखमय कहा जा सकता है और न ही सिर्फ सुखमय।
सत्य तो यह है कि सुखों की अभिलाषा ही वे प्रेरणाएँ है जो व्यक्ति को जीवन के प्रति उत्साहित करती है।
बुद्ध के विचारों में एक अन्य महत्त्वपूर्ण खामी नारियों के अधिकारों के संदर्भ में दिखती है। जैसे महिलाओं को शुरूआत में संघ में प्रवेश नहीं देना।
ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने शिष्य आनंद से कहा था कि अगर संघ में महिलाओं का प्रवेश न होता तो यह धर्म एक हजार वर्ष तक चलता पर अब यह 500 वर्ष ही चल पाएगा।
जबकि वर्तमान में हम देखते हैं कि महिलाएँ हर क्षेत्र में पुरुषों से कंधे से कंधा मिला कर चलने में सक्षम हैं।
महात्मा बुद्ध के विचारों की प्रासंगिकता
महात्मा बुद्ध भारतीय विरासत के एक महान विभूति हैं। उन्होंने संपूर्ण मानव सभ्यता को एक नयी राह दिखाई।
उनके विचार, उनकी मृत्यु के लगभग 2500 वर्षों के पश्चात् आज भी हमारे समाज के लिये प्रासंगिक बने हुए हैं।
वर्तमान समय में बुद्ध के स्व निर्णय के विचार का महत्त्व बढ़ जाता है दरअसल आज व्यक्ति अपने घर, ऑफिस, कॉलेज आदि जगहों पर अपने जीवन के महत्त्वपूर्ण फैसले भी स्वयं न लेकर दूसरे की सलाह पर लेता है अतः वह वस्तु बन जाता है।
बुद्ध का ‘आत्म दीपो भवः’ का सिद्धांत व्यक्ति को व्यक्ति बनने पर बल देता है।
बुद्ध का मध्यम मार्ग सिद्धांत आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना बुद्ध के समय था।
उनके इन विचारों की पुष्टि इस कथन से होती है कि वीणा के तार को उतना नहीं खींचना चाहिये कि वह टूट ही जाए या फिर उतना भी उसे ढीला नहीं छोड़ा जाना चाहिये कि उससे स्वर ध्वनि ही न निकले।
दरअसल आज दुनिया में तमाम तरह के झगड़े हैं जैसे- सांप्रदायिकता, आतंकवाद, नक्सलवाद, नस्लवाद तथा जातिवाद इत्यादि।
इन सारे झगड़ों के मूल में बुनियादी दार्शनिक समस्या यही है कि कोई भी व्यक्ति देश या संस्था अपने दृष्टिकोण से पीछे हटने को तैयार नहीं है।
इस दृष्टि से इस्लामिक स्टेट जैसे अतिवादी समूह हो या मॉब लिंचिंग विचारधारा को कट्टर रूप में स्वीकार करने वाला कोई समूह हो या अन्य समूह सभी के साथ मूल समस्या नज़रिये की ही है।
महात्मा बुद्ध के मध्यम मार्ग सिद्धांत को स्वीकार करते ही हमारा नैतिक दृष्टिकोण बेहतर हो जाता है।
हम यह मानने लगते हैं कि कोई भी चीज का अति होना घातक होता है। यह विचार हमें विभिन्न दृष्टिकोणों के मेल-मिलाप तथा आम सहमति प्राप्त करने की ओर ले जाता है।
महात्मा बुद्ध का यह विचार की दुःखों का मूल कारण इच्छाएँ हैं, आज के उपभोक्तावादी समाज के लिये प्रासंगिक प्रतीत होता है।
दरअसल प्रत्येक इच्छाओं की संतुष्टि के लिये प्राकृतिक या सामाजिक संसधानों की आवश्यकता पड़ती है।
ऐसे में अगर सभी व्यक्तियों के भीतर इच्छाओं की प्रबलता बढ़ जाए तो प्राकृतिक संसाधन नष्ट होने लगेंगे, साथ ही सामजिक संबंधों में तनाव उत्पन्न हो जाएगा।
ऐसे में अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना समाज और नैतिकता के लिये अनिवार्य हो जाता है। इस बात की पुष्टि हाल ही में ‘अर्थ आवर शूट डे’ के रिपोर्ट से होती है जिससे यह पता चलता है कि जो संसाधन वर्ष भर चलना चाहिये था वह आठ माह में ही समाप्त हो गया।
इसे भी पढ़ें
Ranchi Outer Ring Road [रांची आउटर रिंग रोड]-जानियें किन गांवों की जमीन जायेगी